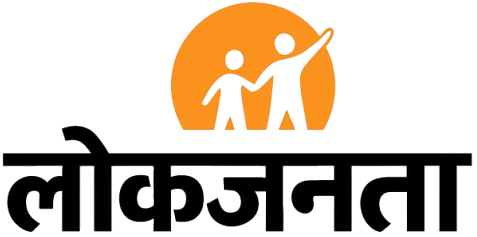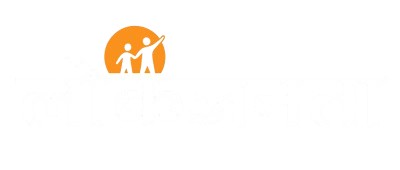लखनऊ: देश की कई हस्तियों के बीच मिमिक्री आम बात है। ऐसा सालों से होता आ रहा है, बल्कि कई सेलिब्रिटीज भी इसका आनंद लेते हैं। जैसे उन्हें शाहरुख खान की हकलाने वाली मिमिक्री से कोई फर्क नहीं पड़ता या नाना पाटेकर की गुस्से वाली मिमिक्री पर वे खूब हंसते हैं, लेकिन बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है. अब डीपफेक के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्हीं की हूबहू छवि में बेतुकी हरकतें या बातें कही जा रही हैं. फर्जी विज्ञापनों में उनके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस वजह से ये सभी सेलिब्रिटीज परेशान हैं. व्यक्तित्व अधिकार को लेकर कई मशहूर हस्तियां- अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, आशा भोसले आदि कोर्ट पहुंच चुकी हैं।
भारत में एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, जो न सरहद पर, न संसद में, बल्कि अदालतों और सोशल मीडिया के बीच लड़ी जा रही है. यह “व्यक्तित्व अधिकार” की लड़ाई है। हाल ही में देश की कई मशहूर हस्तियों अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, आशा भोंसले, सद्गुरु और श्री श्री रविशंकर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्हें किसी शख्स ने मजबूर नहीं किया है, बल्कि एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन लोगों के चेहरे, आवाज और हाव-भाव को इतनी अच्छी तरह से कॉपी किया है कि एक आम नागरिक भी असली और नकली के बीच अंतर नहीं कर सकता है और यही चीज उन्हें मजबूर कर गई है।
AI के आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब किसी व्यक्ति का नाम, चेहरा और आवाज उसकी संपत्ति मानी जाएगी, जिसे वह बेच सकता है, लाइसेंस दे सकता है या इसके इस्तेमाल से रॉयल्टी कमा सकता है?
निजता के अधिकार का उल्लंघन
दरअसल, अब यह बहस सिर्फ निजता तक ही सीमित नहीं रह गई है। मुद्दा यह है कि यदि किसी की पहचान – जैसे चेहरा, आवाज़ या नाम – का उपयोग किसी के आर्थिक लाभ के लिए बिना अनुमति के किया जाता है, तो यह संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। अगर इसका इस्तेमाल किसी को बदनाम करने या अपमान करने के लिए किया जाता है तो इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसका मतलब है कि गोपनीयता उल्लंघन और संपत्ति उल्लंघन के बीच एक सूक्ष्म, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कल्पना कीजिए, आपके इलाके में नाई की दुकान के बाहर अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर लगी हुई है और नीचे लिखा है – “अमिताभ स्टाइल हेयरकट यहां उपलब्ध है!” या फिर कोई आइसक्रीम बेचने वाला जैकी श्रॉफ का डायलॉग बोलता नज़र आ सकता है – “भिडू, यह सबसे स्वादिष्ट स्वाद है जो तुम्हें मिलेगा।” तो यह एक मजाक लग सकता है, लेकिन कानून की नजर में यह व्यक्तित्व अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि इन छवियों या वाक्यों का उपयोग बिना अनुमति के किया गया है।
पहले ये सब इतना गंभीर नहीं माना जाता था. स्टेज शो में अभिनेता फिल्म अभिनेताओं की नकल करते थे, आवाजों की नकल करते थे और मनोरंजन करते थे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक के आने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज और चेहरे को चंद सेकेंड में रीक्रिएट कर सकता है। वीडियो इतनी सटीकता से बनाए जा रहे हैं कि आम दर्शक के लिए असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है.
यही वजह है कि अब अदालतों में नई तरह की याचिकाएं बढ़ने लगी हैं. जैकी श्रॉफ कह रहे हैं कि ‘भिड़ू’ शब्द उनकी पहचान है, अनिल कपूर ‘झकास’ पर अपना हक जता रहे हैं, संजय दत्त ‘बाबा’ शब्द पर अपना दावा कर रहे हैं, तो कोई उनकी तस्वीर या वीडियो के गलत इस्तेमाल से परेशान है. आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिका भी कह चुकी हैं कि लोग बिना इजाजत उनके गानों पर उनकी तस्वीरें लगाकर वीडियो बनाते हैं। यहां तक कि श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु भी अदालत से गुहार लगा रहे हैं कि उनके आध्यात्मिक प्रवचनों का इस्तेमाल उनकी एआई तस्वीरों और आवाजों के साथ किया जा रहा है और जो हमने कहा भी नहीं है वह जनता को बताया जा रहा है, जो न केवल हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का गलत बयानी है, जो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा।
अब यह विवाद भारतीय अदालतों तक पहुंच गया है. कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय अदालतें अब तक इन मामलों में अनुच्छेद 21 यानी जीवन और निजता के अधिकार का सहारा लेती रही हैं। लेकिन यहां एक गहरी दुविधा है. क्या यह “गोपनीयता” का अधिकार है या “संपत्ति” का? अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने इसे संपत्ति के अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया है। वहां मर्लिन मुनरो और एल्विस प्रेस्ली जैसे कलाकारों की मृत्यु के बाद भी उनकी पहचान से जुड़े अधिकार उनके परिवार या ट्रस्ट को मिल जाते हैं, जबकि भारत में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. उदाहरण के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और कहा, “मृत्यु के बाद व्यक्तिगत पहचान स्वचालित रूप से परिवार में स्थानांतरित नहीं होती है।” अर्थात् भारत में व्यक्तित्व अधिकार अभी तक विरासत में नहीं मिले हैं। जब भी कोई नया डीपफेक या अनधिकृत विज्ञापन सामने आता है, तो अदालतों को “जॉन डो ऑर्डर” जारी करना पड़ता है। ऐसे आदेश, जो “अज्ञात व्यक्तियों” के विरुद्ध हों, लेकिन यह समाधान अस्थायी है. यह केवल तात्कालिक राहत प्रदान करता है, स्थायी कानूनी सुरक्षा नहीं। कभी-कभी ये आदेश इतने व्यापक होते हैं कि जायज आलोचना, व्यंग्य और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगने लगता है। परिणामस्वरूप, इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सच तो यह है कि भारत में एआई और डीपफेक के लिए अब तक कोई ठोस कानून नहीं बन सका है। अदालतें मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय दे सकती हैं, लेकिन समग्र नीति नहीं बना सकतीं। इसलिए, अब समय आ गया है कि संसद इस विषय पर एक स्पष्ट और संतुलित व्यक्तित्व अधिकार कानून बनाए, जो न केवल व्यक्ति की पहचान की रक्षा करे, बल्कि कला, व्यंग्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक हित की स्वतंत्रता की भी रक्षा करे।
आलोक तिवारी, लेखक, लखनऊ