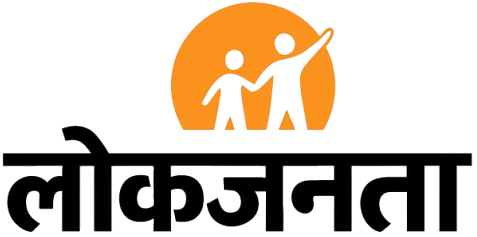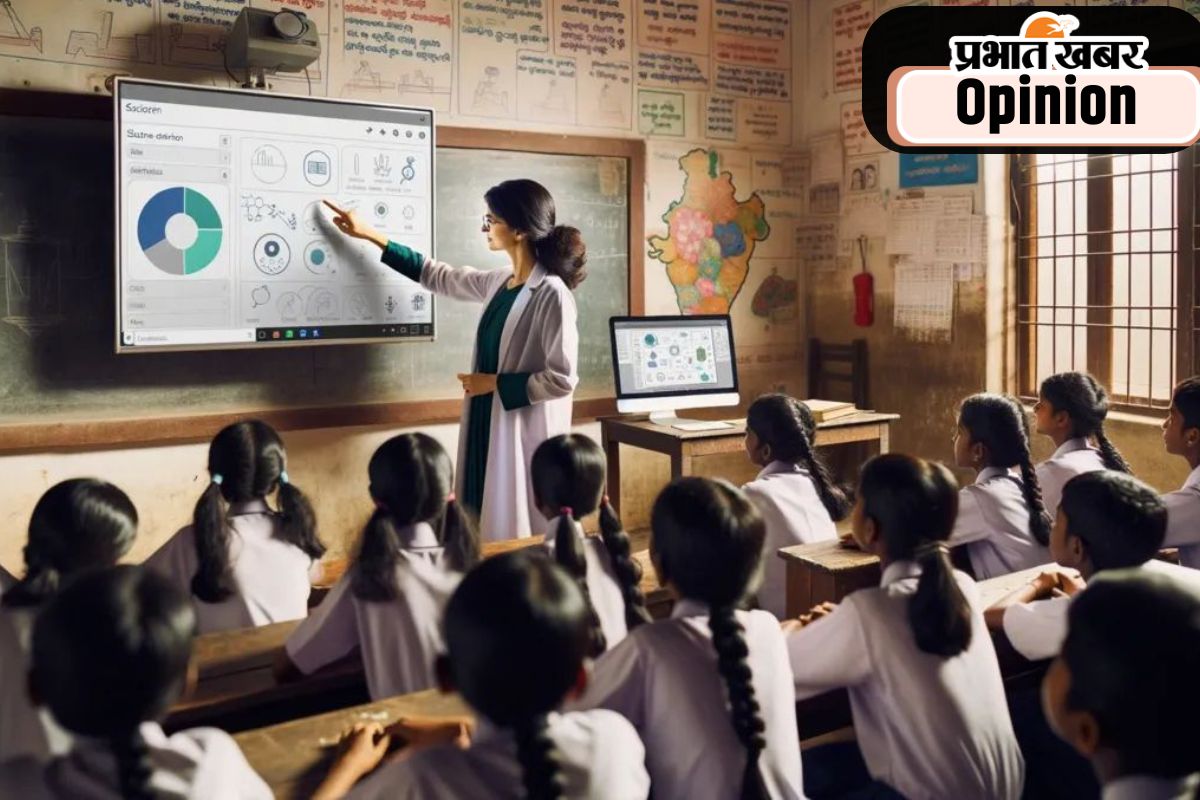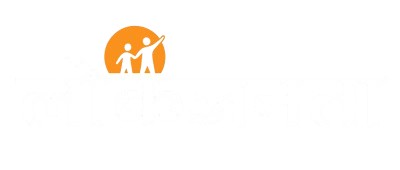Artificial intelligence : तेजी से विकसित हो रही तकनीकी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) अब केवल प्रयोगशालाओं, आइटी या उद्योगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शासन, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है. हाल के दिनों में ऐसी कई पहलें हुई हैं, जो एआइ के मानवीय और कल्याणकारी उपयोग को लेकर हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती हैं. लोकसभा, चुनाव आयोग, और नीति आयोग जैसी प्रमुख नियामक संस्थाओं ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी प्रगति तभी सार्थक होगी जब उसका उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिक और उत्तरदायी ढंग से किया जाये. इन संस्थाओं की साझा सोच दर्शाती है कि भारत न केवल तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करना चाहता है, बल्कि उसे मानवीय मूल्यों, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की कसौटी पर संतुलित भी रखना चाहता है, ताकि एआइ लोकतंत्र को अधिक सक्षम, संवेदनशील और समावेशी बना सके.
हाल ही में बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन) में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एआइ के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि तकनीक को हमेशा मानवता की सेवा में प्रयुक्त होना चाहिए, न कि उस पर नियंत्रण के लिए. उन्होंने बताया कि एआइ जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देने, डिजिटल कनेक्टिविटी को किफायती, समावेशी और जन केंद्रित बनाने के लिए दस लाख से अधिक नागरिकों को नि:शुल्क एआइ प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यह दृष्टिकोण भारत की उस दिशा को परिभाषित करता है जहां तकनीक और मानवीय संवेदना, साथ मिलकर एक नैतिक और समावेशी डिजिटल लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं.
उधर, बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी कि एआइ का दुरुपयोग किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. अब आदर्श आचार संहिता का दायरा केवल पारंपरिक प्रचार तक सीमित न रहकर डिजिटल माध्यमों तक विस्तारित किया गया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की गरिमा और मतदाताओं का विश्वास अक्षुण्ण बना रहे. इसके लिए एक स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट इकाई, त्वरित कार्रवाई व्यवस्था और राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान आवश्यक है. यह पहल न केवल चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली एआइ के दुरुपयोग एवं तकनीकी छल से सुरक्षित, विश्वसनीय और भविष्य संगत बनी रहे.
गौरतलब है कि भारत के लगभग 49 करोड़ असंगठित श्रमिकों का योगदान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के समान है, परंतु सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय स्थिरता जैसी बुनियादी सुविधाओं से वे आज भी लगभग वंचित ही हैं. इसी असमानता को दूर करने के लिए नीति आयोग ने ‘समावेशी सामाजिक विकास हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ शीर्षक से एक ऐतिहासिक रोडमैप जारी किया है, जो भारत को तकनीकी रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य है एआइ, ब्लॉकचेन और इमर्सिव लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से हर असंगठित श्रमिक तक सस्ती, सुलभ और भरोसेमंद डिजिटल सेवाओं को पहुंचाना. नीति आयोग द्वारा बनाया गया ‘मिशन डिजिटल श्रम सेतु’ योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक डिजिटल सामाजिक सुरक्षा पुल का कार्य करेगा. इस मिशन से श्रमिकों को डिजिटल पहचान, कौशल प्रमाणन, रोजगार अवसर, बीमा योजनाएं और वित्तीय सहायता जैसी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में भी एआइ सक्षम मोबाइल प्लेटफॉर्म और भाषायी इंटरफेस के जरिये प्रशिक्षण व जानकारी दी जायेगी, ताकि तकनीक की पहुंच केवल शहरों तक सीमित न रहे.
एआइ का तीव्र प्रसार आज समाज, शासन और अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है. जहां यह नयी संभावनाएं और दक्षता लेकर आया है, वहीं इसके अनियंत्रित उपयोग से चुनावी पारदर्शिता, व्यक्तिगत गोपनीयता, डाटा नैतिकता और सामाजिक असमानता के विस्तार जैसे गंभीर खतरे भी उभर रहे हैं. इस बदलते परिदृश्य में यह प्रश्न पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है कि- तकनीकी प्रगति किसके लिए और किस हद तक?
ऐसे में विभिन्न नियामक संस्थाओं की पहलों का साझा संदेश यही है कि तकनीक केवल उपकरण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है- एक ऐसा माध्यम जो तब तक अर्थपूर्ण नहीं बन सकता, जब तक उसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और नैतिकता का समावेश न हो. भविष्य का भारत केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं, बल्कि नैतिक रूप से परिपक्व डिजिटल राष्ट्र बनकर उभरे, यही इस मानव केंद्रित विकास की मूल भावना है. यह भी गौर करने योग्य है कि भारत ने हाल के दिनों में जिस स्पष्टता और दूरदर्शिता के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के उपयोग को दिशा देने के लिए कदम उठाये हैं, वह न केवल एक राष्ट्रीय नीति-संकल्प है, बल्कि एक वैश्विक संदेश भी है. जाहिर है कि भारत एआइ को अंधाधुंध अपनाने के बजाय, इसे मानवीय मूल्यों और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ संतुलित करना चाहता है.
(ये लेखक के निजी विचार हैं.)