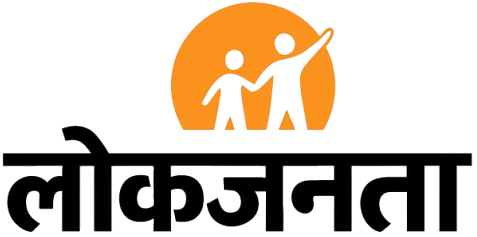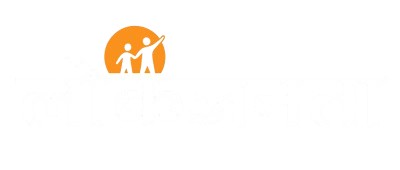सर्दियों के महीनों के दौरान आमतौर पर कुछ दिन कड़ाके की ठंड पड़ती है। कभी-कभी यह चालीस दिन का होता है, जिसे चिल्ला जाड़ा कहा जाता है। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पैनल की नवीनतम रिपोर्ट में जो कहा गया है, उससे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दशकों में शीत लहर और कठोर सर्दियों की समस्याएं अतीत की बात हो जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 से 2020 के बीच, यानी पिछले चालीस वर्षों में, अत्यधिक ठंडी रातों और बहुत ठंडे दिनों की संख्या में चार गुना कमी आई है, जबकि अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।
वर्ष 2100 तक सर्दी लगभग गायब हो जाएगी। यह बदलाव सिर्फ मौसम में उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में गहरे असंतुलन का संकेत है, जिसका देश के पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाला है। गर्म दिनों का मतलब ऊर्जा की मांग में भारी वृद्धि है, जिससे उत्पादन लागत और बिजली की कमी दोनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में गर्मी और लू से मौतें बढ़ेंगी.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में गर्मी से संबंधित बीमारियों और मौतों की दर अगले दो दशकों में दोगुनी हो सकती है। बाढ़ की आवृत्ति भी बढ़ेगी. इसका असर पहाड़ी इलाकों पर दिखने लगा है. बर्फ की परतें पिघल रही हैं, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और नदियों का प्राकृतिक जल प्रवाह असंतुलित हो गया है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। यहां ग्रामीण जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों इससे प्रभावित हैं। जिन फसलों, फलों और फूलों की खेती ठंड के मौसम पर निर्भर थी, उनकी पैदावार घट रही है। पारंपरिक बागवानी बेल्ट के अधिक ऊंचाई की ओर स्थानांतरित होने के कारण छोटे किसानों की आजीविका खतरे में है। तापमान में वृद्धि के कारण कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जो फसलों के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसके कारण असंतुलित जल चक्र ने मानसून के पैटर्न को बदल दिया है, जिसके कारण सूखा और अत्यधिक वर्षा आम होती जा रही है।
यदि नदियों के प्रवाह में कमी और जल स्रोतों के सूखने से पेयजल संकट बढ़ेगा, तो गर्मी की लहरों, जंगल की आग, चक्रवात और भूस्खलन की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। देश की जन-धन की अरबों रुपये की हानि होगी। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण प्राधिकरण पहल और मिशन लद्दाख हिमालय जैसी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जिस गति से आपदा बढ़ रही है, उसे देखते हुए उनकी गति और दायरा अभी भी पर्याप्त नहीं है। सरकारों को समय रहते दीर्घकालिक और बहुस्तरीय तैयारी करनी होगी। पहाड़ी राज्यों में जलवायु अनुकूल कृषि, जल संरक्षण, ग्लेशियर निगरानी प्रणाली विकसित करनी होगी, शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा कुशल भवनों को बढ़ावा देना होगा। स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना और गर्मी से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करना जरूरी है। सच तो यह है कि संकट आसन्न है, इसलिए जब तक पर्यावरणीय चेतना को शासन की प्राथमिकता में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इस पर्यावरणीय खतरे से निपटना मुश्किल होगा।